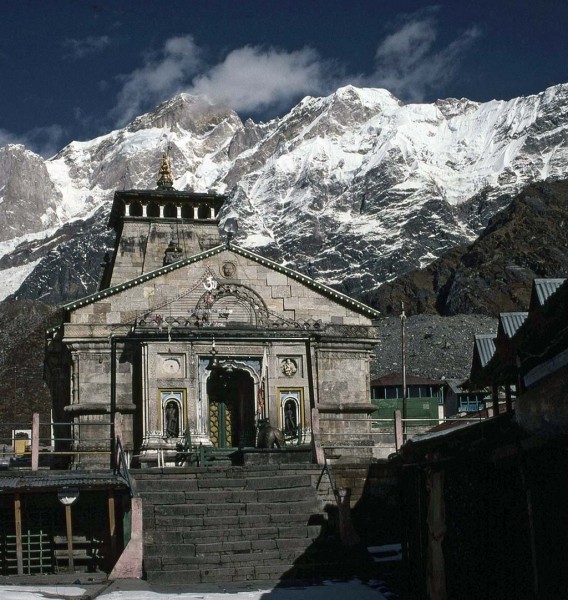उस दिन बैठे-ठाले, बस यूँ ही पलकों से टीवी खुरच रहा था. टीवी में न्यूज़ चैनल उस सावन जैसे हैं जिसके आते ही व्यर्थ-निरर्थक सोच के बादल उमठना शुरु हो जाते हैं. शाहीनबाग़ के बाद दिल्ली की एक और घेराबन्दी चल रही थी. इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक की जाट-लैण्ड का किसान समुदाय ‘कृषिक्षेत्रे शासनक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः’ हुआ आन्दोलन कर रहा था. मुझे लग रहा था हम हिन्दुस्तानियों को अभी तक एक संविधान के अधीन एक राष्ट्र की तरह उपक्रम करने की आदत नहीं पड़ी है. दुनिया भर में हमारे मुसलिम भाइयों की तो एक ‘उम्मत’ होती है – नबी की उम्मत, मगर हम हिन्दुस्तानियों की ‘उम्मत-ए-हिन्द’ के अब तक पते नहीं हैं. प्रान्त, जाति, भाषा, व्यवसाय, राजनीति आदि की इतनी उम्मतें हैं कि हम अपने-अपने गुट को उम्मत का दर्जा देकर जब-तब सिर-फुटव्वल में मशगूल रहते हैं.
टीवी के बादलों में बिजली तो क्या कड़कती, बग़ल में रखा फ़ोन गरजने लगा.
बादलों को हथेली से एक तरफ़ सरकाया और रिमोट रखकर फ़ोन उठाया. देखा तो मित्रवर महेन्द्र मोदीजी!
आकाशवाणी में जब नौकरीशुदा थे, रिटायर नहीं हुए थे, तब इस महावृक्ष ने चिन्तन-दर्शन-कर्मण के जाने कितने बीज हम लोगों के जीवन के भू-विस्तार में छितराये. वे बीज अलग-अलग परतों में दबे-ढँके सोये रहते हैं.
महेन्द्र जी ने बताया ‘रेडियोनामा’ सीरीज़ की चौथी पुस्तक “ले बाबुल घर आपनो” उन्होंने लिखकर पूरी कर ली है और उसकी ‘प्रस्तावना’ मुझे लिखनी है.
महेन्द्र मोदी जी की बात और पांडुलिपि पढ़ने का अवसर मिला तो उसने जो रिमझिम कर दी उन छींटों से कुछ बीजों की नींद टूटी और मन की परतें फोड़कर चंद कोंपलें उचक आयीं. उन सब को समेटा और ‘बरबादियों का जश्न’ शीर्षक की गाँठ से बाँधकर महेन्द्र जी के हवाले कर दिया.
वे मुट्ठी-भर विचार उस पुस्तक की ‘प्रस्तावना’ बन गए जो यहाँ दे रहा हूँ.
मिर्ज़ा ग़ालिब जैसे कवि के सामने मेरे जैसे अकिंचन ज़रूर क़तरा हैं. मगर भले ही बढ़ रही उम्र के चलते हाथ में जुंबिश कम होती जाती हो, लिखने-पढ़ने का रसिया होने से ऐसे किसी अवसर के साग़र-ओ-मीना सामने आते ही मेरी आँखों को याद आ जाता है उनमें अभी दम बाक़ी है.
जब मैंने इस पुस्तक की पाण्डुलिपि पढ़नी शुरु की तो मित्र-धर्म पीछे छूट गया. ज्यों-ज्यों आगे पढ़ता गया मुझे स्पष्ट होता गया कि मैं एक मित्र की पाण्डुलिपि पढ़कर कोई अहसान नहीं कर रहा था, बल्कि एक ज़ोरदार सत्यकथा पढ़ रहा था! ऐसी कथा जिसकी घटनाएं, वास्तविक पात्र और पेंचदार परिस्थितियाँ पाठक के ऊपर कई स्तरों पर काम करने जा रही हैं. जो लोग रेडियो को – आकाशवाणी – को अन्दर से जानते हैं, उनपर एक ख़ास तरह से; जो सामान्य पाठक हैं उनपर दूसरी तरह से; और जो केवल एक ऐसे जीवन-चरित्र में कुतूहलवश दिलचस्पी रखते हैं जो अपनी आवाज़, रेडियो के माध्यम और फ़ोटोग्राफ़ी से प्रसिद्ध हो गया हो, उनपर अलग तरह से.
यहाँ ‘जीवन-चरित्र’ कहना शायद भ्रामक होगा. व्यक्ति को जानने और उसके माध्यम से जीवन को समझने के मुख्य रूप से तीन साधन हैं – जीवन-चरित्र, आत्मकथा और संस्मरण/डायरी. ‘जीवन-चरित्र’ उसे कहेंगे जब किसी का जीवन-वृत्त कोई दूसरा व्यक्ति लिखे. ‘आत्मकथा’ में अपने जीवन की गाथा व्यक्ति स्वयं कहता-लिखता है. जब जीवन में आये व्यक्तियों, घटे हुए प्रसंगों, यात्राओं, मुलाक़ातों आदि के बारे में विशेष प्रसंग चुनकर लिखा जाता है तो उसे ‘संस्मरण’ कह दिया जाता है. इन्हें बहुधा ‘डायरी के पन्ने’ भी कहा गया है.
आत्मकथ्य का यों भी एक-स्तरीय हो पाना मुमकिन नहीं है. व्यक्ति भले एक हो, जीवन की बल खाती-इठलाती-बदलती परिस्थितियाँ कितने ही वातायन खोलती चलती हैं. जैसे कि एक ही मकान के अनेक खिड़की, दरवाज़े, रोशनदान! अलग-अलग कमरों की अलग-अलग दीवारें, छतें और फ़र्श!!
‘रेडियोनामा’ की पहली तीन पुस्तकों और अब इस चौथी कड़ी में लेखक श्री महेन्द्र मोदी ने आत्मकथा के पुष्प और यथा-प्रसंग संस्मरण के मोती पिरोकर माला सजायी है. इस सीरीज़ में ‘आत्मकथा’ की सुवास और ‘संस्मरण’ की छटा दोनों एक साथ विद्यमान हैं.
‘रसीदी टिकट’ शीर्षक से पंजाबी की वरिष्ठ लेखिका अमृता प्रीतम की आत्मकथा बहुचर्चित हुई थी. बाद के संस्करणों में अमृताजी ने उसे काट-छांट कर बहुत कम कर दिया था और इसका कारण बताते हुए कहा था – “कई घटनाएं जब घट रही होती हैं, अभी-अभी के ज़ख्मों-सी, तब उनकी कोई कसक अक्षरों में उतर आती है… लेकिन वक़्त पाकर अहसास होता है कि ये बातें, लम्बे समय के लिए साहित्य को कुछ दे नहीं पायेंगी… ये वक़्ती आँधियाँ होती हैं…”
वक़्ती यानी सामयिक, तात्कालिक.
यों देखें तो हर क्षण ‘वक़्ती’ है. वक़्त के गुज़रने का अर्थ ही है क्षण का सरक जाना. उस फिसलते क्षण में व्यक्ति जब दूरगामी परिणामों पर असर डालने वाले निर्णय लेकर आचरण करता है तो उसका वक़्ती आचरण समय की थाती बन जाता है, हवाओं पर छप जाता है.
दरअसल महेन्द्र मोदी जी अपनी कथा तो कह ही रहे हैं, जीवन की भी बात कर रहे हैं. जब लेखक व्यक्ति की तरह नहीं यायावर की तरह जीवन-प्रान्तर में घूम रहा हो और अपने आप से फ़ासला रखकर शाब्दिक फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हो तो उसके पास व्यक्तिगत आग्रहों के लिए फ़ुर्सत ही कहाँ होती है? ऐसा करते हुए मोदीजी ने लगातार ‘फ़्लैश बैक’ और ‘फ़्लैश फ़ारवर्ड’ का भरपूर इस्तेमाल किया है. आग्रह-युक्त और उसी क्षण में आश्चर्यजनक ढंग से आग्रह-मुक्त वर्णन होने के कारण पाठक को यह परेशानी नहीं होने पाती कि वर्त्तमान से अचानक बीस बरस आगे या दस वर्ष पहले की बात कैसे होने लगी. सब कुछ हवाओं पर छपता चल रहा है. कभी इस झोंके पर, कभी उस झकोरे पर.
जो और जैसे व्यक्ति लेखक को मिले, जो परिस्थितियाँ बनी-बिगड़ीं, जिसने जैसा किया, उन हालात में जो कुछ हुआ, जो ‘लै बाबुल घर आफ्नो’ में, पहले के भागों में भी पढ़ने को मिलता है, वैसा क्योंकर हुआ होगा, उसे समझने के लिए लेखक महेन्द्र मोदी को व्यक्ति महेन्द्र मोदी की तरह समझना, और उसके बाद यायावर की तरह देखना सहायक होगा.
सोचते-सोचते मुझे एक कहानी याद हो आयी. कहानी हमारा सबसे बड़ा गुरु है. जो सबक हम उपदेश में सुनकर ऊब जाते हैं और भूलने को तत्पर होते हैं, कहानी वही शिक्षा हमें सहज दे जाती है. हमेशा के लिए.
एक किसान का बेटा कृषि विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर गाँव लौटा. फ़सल की आगामी बुवाई में पिता का हाथ बँटाते हुए ग्रेजुएट बेटे ने कहा, “बापू, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं. लेकिन कभी बेवक़्त बारिश तो कभी आँधी और कभी लगातार चिलचिलाती धूप! अक्सर हमारी मेहनत बेकार चली जाती है.”
पिता ने लम्बी साँस भरते हुए कहा, “अब जैसी परमात्मा की मर्ज़ी बेटा.”
बेटे ने कहा, “अगर एक साल, सिर्फ़ एक साल आपका यह परमात्मा मेरे काम में दख़ल न दे तो मैं इसी खेत में चमत्कार कर सकता हूँ. वरना इतनी पढ़ाई का फ़ायदा ही क्या?”
परमात्मा लड़के की बात सुन रहा था. उसकी इच्छा जानकर वहाँ प्रकट हो गया.
लड़के ने पूछा, “सर, इतना मेकअप करके, इस नौटंकी वाले कॉस्टयूम में आप कौन? और आप अचानक कहाँ से प्रकट हो गये?”
“मैं परमात्मा हूँ और तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ. बोलो पुत्र, क्या चाहते हो?”
लड़के को देखकर साफ़ पता चल रहा था कि वह अपनी हैरानी कम, अविश्वास अधिक छुपाने की कोशिश कर रहा था. फिर भी, एटीकेट-वश बोला, “ऐसा ही है सर, तो एक वर्ष के लिए मुझे अपने आँधी-पानी-ताप-धूप वगैरह से मुक्त कर दीजिये. मैं शानदार फ़सल उगाकर पूरे ज़माने को दिखाना चाहता हूँ.”
‘तथास्तु’ कहकर परमात्मा अन्तर्धान हो गया.
अब तो लड़का लग गया जी-तोड़ मेहनत करने में. पूरी तरह नियन्त्रित तापमान, ज़रूरत जितने नपे-तुले पानी की सिंचाई, उचित प्रकाश, अनुकूल छाया आदि का बंदोबस्त करके लड़के ने फ़सल उगाई. समय पाते उसके खेत की फसलें बढ़ चलीं. अगल-बग़ल के खेतों में फसलें अगर चार फ़ीट की तो उसके खेत में आठ फ़ीट ऊँची. दूसरों के यहाँ बालियाँ बालिश्त भर की तो उसके खेत में दो-दो फ़ीट लंबी. पूरा गाँव तारीफ़ के बोलों और ईर्ष्या भरी निगाहों से देखता हुआ ग्रेजुएट लड़के के कृषि-ज्ञान से प्रभावित हुआ घूमे.
फ़सल कटाई का समय आया तो परमात्मा फिर प्रकट हो गया. लड़के की प्रशंसा करते हुए बोला, “वाक़ई, तुमने कमाल कर दिखाया है. ज़रा बालियों का दाना भी देखें.”
लड़का मुट्ठी-भर बालियाँ काट लाया. छील कर देखा तो दाना एक नहीं. दूसरे कोने से और बालियाँ लाया. उनमें भी एक भी दाना नहीं. और लाया तो वे भी छूँछी!
लड़का सिर पकड़ कर बैठ गया.
ईश्वर बोला, “पुत्र, ये फ़सलें आँधी-पानी, धूप-बादल और हवाओं से जितना संघर्ष करती हैं, इनमें दाना उससे आता है. तुमने इनका संघर्ष छीनकर इन्हें दाने से वंचित कर दिया.”
इस पुस्तक के लेखक ने जितना संघर्ष झेला, ईर्ष्या, उपेक्षा, षड्यंत्र का सामना किया, चुनौतियों में छलांग लगायी, अधिकारों से वंचित हुआ उसी सब से महेन्द्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति बने जिसमें हर परिस्थिति का सामना करने की कूव्वत हो, डट जाने का संकल्प हो, बात निभाने का माद्दा हो और जब उचित लगे तब टाल जाने का बड़प्पन भी हो. आवाज़ और प्रतिभा तो कुदरत की दी हुई है ही.
‘ले बाबुल घर आफ्नो’ ऐसे ही ‘दाना-दार’ इनसान की कहानी उसकी अपनी ज़ुबानी है.
आम तौर पर मीडिया का काम इतने तक माना जाता है कि किसी विषय या समस्या के विभिन्न पहलू आम श्रोता के सामने लाने के बाद निष्कर्ष अथवा परिणाम पर पहुँचना श्रोता पर ही छोड़ दे. ऐसा आदर्श स्थापित है कि प्रो-एक्टिव होकर समस्या को हल की ओर ले जाना मीडिया का दायित्व नहीं होना चाहिए.
मगर मोदीजी इस पुस्तक में सामाजिक समस्याओं पर कार्यक्रम करते हुए उन्हें किसी सार्थक निष्कर्ष तक ले जाने की कोशिश करते दिखेंगे. यहाँ तक कि ड्रग्स जैसे नशे की बुराई की जड़ तक जाते हुए जान का ख़तरा तक मोल लेते दिखाई देंगे. क्योंकि समाज को समस्या से निजात दिलाना उन्हें अपने काम को पूरा करने जैसा लगा. वर्ना काम अधूरा.
इससे पहले कि ऐसा करना किसी को अति-उत्साह जैसा लगने लगे इस विषय पर और विचार करना उपयुक्त होगा.
आम तौर पर हम सभी में एक वृत्ति, एक मनोविज्ञान सक्रिय रहता है. बड़ी संख्या में समाज के लोगों को परेशान करने वाली कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हम किनारे खड़े रहकर ईश्वर की तरह तमाशबीन हो जाना पसंद करते हैं. हम भूल जाते हैं कि जब तक मंसूर की मानिंद ‘अन-अल-हक़’ का अनुभूति-जन्य सत्य हमारा स्पर्श न कर ले, हम ‘अहं ब्रह्मास्मि’ कहने के हक़दार नहीं हो जाते. तब तक हम ईश्वर नहीं, मनुष्य हैं, और मनुष्य का काम तमाशा देखना नहीं है. वह तमाशे की पुतली हो जाने को अभिशप्त है.
उदाहरण के लिए एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो ऑफ़िस जाने के लिए घर से निकलता है, थोड़ी हड़बड़ी में है, शायद थोड़ा लेट हो गया है, मगर बस स्टॉप के रास्ते में दो आदमियों को मारामारी करते देखता है. ऑफ़िस के लिए हो रही देरी भूलकर वह उन दोनों का झगड़ा देखने के लिए वहीं रुक जाता है. थोड़ी देर में वहाँ अच्छी-ख़ासी भीड़ जमा हो जाती है जिनके लिए वहाँ चल रही मार-धाड़ एक तमाशा है. लड़ने वाले दोनों व्यक्ति भी इतने लोगों को जमा हो गया देखकर हीरो हो जाने के लिए विरोधी को परास्त करने में पूरी ताक़त लगाने लगते हैं. हिंसा की मंशा और ज़ोर पकड़ लेती है.
यह एक काल्पनिक दृश्य भले हो, किन्तु ऐसा वास्तव में होता हुआ हम में से हर किसी ने कभी-न-कभी अवश्य देखा होगा. यहाँ विचार करने की बात यह है कि वहाँ इकट्ठा हो गई भीड़ में से किसी के भी लिए वहाँ हो रही हिंसा ऐसा मामला नहीं थी जिसे सुलझाया जाए. उलटे, उस भीड़ के हर व्यक्ति में झलकती उत्सुकता उस आग में और ईंधन डालने का काम कर रही थी. क्या हमने कभी सोचा है कि अन्य भी सभी समस्याओं में हमारी तटस्थता इसी तरह हमारे जाने-अनजाने उस समस्या को और बढ़ाने का कारण बनती चली जाती है? यह हमारी शराफ़त या निर्लिप्तता का नहीं, सामाजिक समस्याओं को गहराने में हमारे योगदान का प्रमाण है.
तमाशे का हिस्सा हो जाने का अर्थ यह कैसे हो गया कि यदि मार-पीट हो रही है तो उसमें शामिल हो जाएं? यह क्यों नहीं कि हिंसा की अग्नि को बुझाने वाले बन जाएं? अन्याय या शोषण है तो उस स्थिति में कूद जाने का यह अर्थ क्यों नहीं हो जाता कि वैसी मनोवृत्ति को अर्थहीन बनाने में जुट जाएं? ऐसा न हुआ तो एक मीडिया-कर्मी और एक माफ़िया-डॉन के बीच का फ़र्क कैसे तय होगा? बुद्धिजीवी और जगत्गति न ब्यापने वाले मूढ़ में क्या अन्तर रह जाएगा? क्या हम बुद्धिजीवियों की इस क़दर मानसिक कण्डीशनिंग हो चुकी है?
कम-से-कम यह मुझे सिर झटक कर टालने जैसी बात नहीं लगती.
यदि हमारे मित्र, इस पुस्तक के लेखक श्री महेंद्र मोदी स्वभाव-वश अपने आचरण से यह बता रहे हैं कि प्रो-एक्टिव होकर समस्याओं को सुलझाना हर व्यक्ति का नहीं तो कम-से-कम बुद्धिजीवियों और मीडिया का उत्तरदायित्व अवश्य है तो इसे अति-उत्साह नहीं, ग्रहण करने योग्य चरित्र कहना सम्यक् होगा.
इस तरह लेखक से एक काम और हो गया है. वह भी शायद अनजाने में, सहज रूप से.
ज़रा पुराने रेडियो सेट को याद कीजिये. ट्रांज़िस्टर-युग से भी पहले वाले रेडियो को, जिसमें वाल्व होते थे और कमरे की छत के पास इस दीवार से उस दीवार तक एरियल लगाना पड़ता था. मुझे अपने बचपन की याद हो आयी जब हमारे घर का ऐसा ही रेडियो सेट बिगड़ गया था. घर का बड़ा बेटा होने के नाते उसे ठीक करवाकर लाना मेरा काम था. यों भी, वह रेडियो जिस टेबिल पर रखा रहता था मैं वहीं बैठकर स्कूल की पढ़ाई, होमवर्क आदि किया करता था. जिन घरों में तब रेडियो था, वहाँ रेडियो सुनना एक आदत बन जाती थी. मुझे भी रेडियो चलाकर पढ़ाई करने की आदत हो गयी थी. इसलिए उस रेडियो के आकाश का पुनः वाणीमय हो जाना घर भर में सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी. रेडियो की ख़ामोशी मेरे लिए ऐसी हो गई मानो स्कूल से मेरा नाम कट गया हो!
लिहाज़ा मैं रेडियो सेट उठाकर विक्रेता के पास ले गया. उसके टेकनीशियन ने यह देखने के लिए क्या गड़बड़ है उसे पीछे से खोला. बाहर से तो हम रेडियो को बड़े चाव से झाड़-पोंछ कर चमकाकर रखते थे. मगर अन्दर का नज़ारा कुछ और ही था. अन्दर देखा तो धूल और जालों ने अपनी पूरी दुनिया बसा रखी थी. कौन सा तार कहाँ से किधर जा रहा है, समझना मुश्किल था. काँच के वाल्व माया की मीनारों जैसे लग रहे थे. वहाँ तो जैसे एक तिलिस्मी प्रपंच रचा हुआ था!
कुछ इसी तरह का हाल आकाशवाणी का भी कहा जा सकता है. एक आम श्रोता तो धुली-पुंछी आवाज़ें, सधे हुए कार्यक्रम और गुनगुनाता संगीत ही सुनता है. अन्दर कितनी धूल होगी, कहाँ-कहाँ कितने जाले लगे होंगे, किस महानुभाव के तार किस अफ़सर से जुड़ते होंगे और क्यों, उसे क्या मालूम! वह नहीं जानता कितने तरह के कर्मचारी होंगे, उनमें से कितने लोग कार्यक्रम तैयार करते होंगे, कितने प्रशासन चलाते होंगे और कितने महज़ क्लर्की करते होंगे. किसी श्रोता को जानकर करना भी क्या है कि इस विभाग में लोगों की भरतियाँ कैसे होती हैं, जब तक कि उसकी ख़ुद की दिलचस्पी आकाशवाणी का कलाकार हो जाने की न हो जाती हो. इंजीनियर वर्ग की पहली पसन्द नौकरी के लिए चुने जाने के बाद रेलवे अथवा डाक-तार-टेलीफ़ोन विभाग में नियुक्ति की होती थी. आकाशवाणी तो तीसरे नम्बर पर आती थी. यांत्रिक जगत् में कैरियर को प्राथमिकता मिलना स्वाभाविक था.
घटनाचक्र को उकेरते हुए श्री महेन्द्र मोदी ने भीतर के जाल-जंजाल की भी झलक दे दी है. इतनी साफ़गोई से इन बातों को कोई ‘दाना-दार’ व्यक्ति ही कह सकता था.
मेरा स्वयं का भी मानना यही है कि आकाशवाणी, जो कि कला-साहित्य-संस्कृति से सम्बन्धित होने के कारण निस्संदेह देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था थी, उस दिन से पतन की फिसलती ढलान पर आ गयी जिस दिन से व्यक्तियों (कर्मचारियों-अधिकारियों) के चयन में प्रमाद होना आरम्भ हुआ. शिक्षा एवं सूचना-प्रसारण कोरा व्यवसाय नहीं, उससे बहुत आगे की चीज़ हैं. इन क्षेत्रों में प्रवेश केवल नौकरी के लिए नहीं, समाज के नैतिक नेतृत्त्व के लिए हो, इसका तर्क नहीं होता. केवल औचित्य होता है. जब आकाशवाणी मात्र एक नौकरी हो गई तो पदोन्नतियाँ भी वरिष्ठता-सूची के क्रमांक से होंगी. गोया स्कूली बच्चों के रोल नम्बर से उनकी हाज़िरी लगायी जा रही हो! मुझे नहीं लगता ‘रघुवंश’, ‘शाकुंतलम्’ या ‘मेघदूत’ लिखना कालिदास की ‘नौकरी’ थी. या फिर ‘ओथेलो’, ‘हैमलेट’ या ‘किंग लीयर’ लिखने की ‘हैसियत’ शेक्स्पीयर में इसलिए बन गयी थी कि उनका रोल नम्बर आ गया था.
आप किसी को भी केन्द्र निदेशक-महानिदेशक कुछ भी बनाइये, किसी भी केडर से व्यक्ति का चुनाव कीजिये, मगर यह ज़रूर देख लीजिये कि वह जगदीशचन्द्र माथुर या हरिश्चंद्र खन्ना है या नहीं! अनमने भाव से ‘कैरियर प्रथम’ वाले इंजीनियरों का मूल्य उनकी प्रतिभा और शिक्षा के परिमाण में अवश्य आँका जाए, किन्तु आकाशवाणी जैसे संस्थान के केंद्र पर विभागाध्यक्ष? केंद्र-संचालक? आकाशवाणी का महानिदेशक?
ऐसी स्थिति के लिए मैंने अपने एक अन्य लेख में जो उदाहरण दिया है, मुझे लगता है उसे यहाँ भी दोहरा देना चाहिए.
रद्दीवाला याद है आपको? घर-घर से पुराने अख़बार की रद्दी व अन्य बेकार सामान उठाने वाला कबाड़ी? अब तो वह डिजिटल काँटा लाने लगा है, मगर कभी वह तराज़ू और बाट लेकर चलता था. एक पलड़े में एक किलो का बाट रखता और दूसरे में उतने अख़बार रखकर तौलता. फिर उन्हें बाट वाले पलड़े में रखकर दो किलो बना लेता था. फिर दो किलो तौलकर चार किलो बना लेता था. दोनों पलड़े के आठ किलो उठाना मुश्किल लगता तो हौले से एक किलो वाला लोहे का ओरिजिनल बाट निकालकर एक तरफ़ सरका देता था.
और चल पड़ता था रद्दी से रद्दी तुलने का सिलसिला!
हमारी प्रिय आकाशवाणी में भी भरती और प्रमोशन जब रद्दी से रद्दी तौलकर होने लगे तो जो हो सकता था वही हुआ!
श्री महेन्द्र मोदी ने कितना भी क्षुब्ध होकर इस स्थिति पर सवाल उठाया हो, उनकी यह बात हर किसी के द्वारा ध्यान दिये जाने की दरकार रखती है.
जिन लोगों ने एकहार्ट टॉल की पुस्तक ‘द पॉवर ऑफ़ नाओ’ पढ़ी है, वे जानते हैं यथार्थ क्या है और भ्रम क्या. टॉल ने ‘ब्रह्म सत्यम् जगत् मिथ्या’ की पहेली को बहुत सरल करके समझा दिया है कि सत्य क्या, मिथ्या क्या है.
आधी रात के बाद कभी अचानक नींद उचट जाए तो हम पाते हैं कि घोर नि:स्तब्धता छायी हुई है. घुप्प चुप्पी! यदि अचानक निकट के हाईवे पर कोई वाहन गुज़र जाए या कोई कुत्ता भौंक दे तो उसकी आवाज़ ज़रूर सन्नाटे की ख़ामोश लहरों पर तैरती हुई हम तक आ जाती है. लगातार पसरे सन्नाटे के विस्तृत आकाश में यह एक ध्वनि बादल के टुकड़े की तरह प्रकट हुई और फिर उसी मौन में बिखर कर लुप्त हो गयी. वाहन की या भौंकने की आवाज़ ने आकर बताया कि यह आवाज़ जिसमें तैरी वह अनन्त मौन इस आवाज़ के आने के पहले भी था और लुप्त हो जाने के बाद भी है. ठीक से देखें तो आवाज़ ने प्रकट होकर हमें सन्नाटे के लगातार होने का अहसास कराया! यदि ये शब्द प्रकट न होते तो हमारे लिए अप्रकट मौन का होना एक शब्द-हीनता मात्र होता.
इसी तरह जब हम अपने लिए कोई नया मकान या फ़्लैट देखने जाते हैं तो हमारा सामना पूरी तरह ख़ाली पड़े कमरों से होता है. हमारा सामान और फ़र्नीचर उस ख़ाली को, उस अवकाश, उस आकाश को उस दिन भरेगा जब हम इस फ़्लैट को ख़रीद कर उसमें रहने आ जायेंगे. फ़र्नीचर वहाँ होकर यह बतायेगा कि हमारी टेबिल और कुर्सी, पलंग और अलमारी उसमें हैं जो सब तरफ़ पसरा आकाश — अवकाश, शून्य, ख़ालीपन – है!
शब्द अथवा मेज़ का होना और कुछ नहीं मौन और शून्याकाश के परिचय-सूत्र हैं. जो आते-जाते हैं, हटते हैं, विलीन होते हैं वे फ़र्नीचर या शब्द हैं. शून्य और मौन तो वहीं रहते हैं. अब यह हमारी मानसिक कण्डीशनिंग का आलम है कि हमारा ध्यान सदा लय हो जाने वाली मेज़-कुर्सी-अलमारी या ध्वनि पर केन्द्रित रहता है. वस्तुतः जो ख़ालीपन अथवा सन्नाटा है उस पर तब केन्द्रित होना शुरु होता है जब फ़र्नीचर या शब्द से हमारा रिश्ता बनता है.
यह भी अवश्य हमारी मानसिक कण्डीशनिंग ही कही जाएगी कि हम इस पुस्तक में वर्णित घटनाओं के घात-प्रतिघात और उनके लब्ध पर केन्द्रित होने को चुन लेंगे – अमुक व्यक्ति ऐसा निकला, ऐसी-ऐसी नीति ने वैसा-वैसा परिणाम ला दिया, किसी-किसी शहर की ‘कल्चर’ ऐसी है, आदि आदि. फिर हो सकता है हम यह भी कहें कि हमें तो मालूम नहीं, महेंद्र मोदी ने अपनी किताब में ऐसा बताया है.
जबकि हमारा ध्यान केन्द्रित होना चाहिए उस जीवन पर जो लेखक के इर्द-गिर्द पसरा रहा है. स्थितियाँ-परिस्थितियाँ बनकर मौजूद रहा है. अन्ततः लेखक का जीवन, किसी भी व्यक्ति का जीवन अनन्त आकाश की तरह है. घटनाओं का उपलब्ध अथवा हाथ में आये परिणाम पसरे हुए सन्नाटे में उगे शब्द की तरह हैं, कमरे के ख़ालीपन में दिखे फ़र्नीचर की तरह हैं. निष्पत्तियों के रिश्ते से वास्तव में हमें देखना तो जीवन के विस्तार को है!
निष्पत्तियों का – व्यक्तियों की कमज़ोरियों, झूठ, कपट, लोभ, भ्रष्टाचार, पक्षपात आदि को कहने का अर्थ है यह बताना कि उनका कोई स्थायी महत्त्व नहीं है, वरना लेखक उन्हें कहता ही क्यों? ‘लै बाबुल घर आपनो’ कहकर उसने इस ‘प्रकट’ अस्थायित्व को जीवन की सच्चाइयों के आधारभूत (अप्रकट) कैनवस पर चित्र की तरह उकेर दिया है.
इस किताब का पढ़ना इस पर निर्भर रहेगा कि हमारा ध्यान किस पर केन्द्रित है – घटनाओं और उनकी परिणति पर, अथवा उस सत्य पर जिसके आकाश में ये ‘प्रकट’ जुगनू टिमटिमाये हैं.
जो पाठक सदा से, बहुत पहले से रेडियो सुनते आये हैं वे इस बात की साक्षी देंगे कि फ़िल्मी गीतों में यदि कोई शायर वेदान्त को उतार पाया तो वह थे साहिर लुधियानवी. संसार की हर शै को इक धुन्ध से आना है और इक धुन्ध में जाना है कहने वाले इस कवि ने अपने एक गीत में यह भी कहा था कि बरबादियों का सोग मनाना फ़िजूल था, बरबादियों का जश्न मनाता चला गया!
इस पुस्तक के सब हासिलों, हर उपलब्धि, विभिन्न निष्कर्षों को लेखक ने अनन्त में लय हो जाने वाली बरबादियों की तरह देखा है जिनका सोग मनाना फ़िजूल है. इसलिए लेखक जीवन के सिरजनहार से कहता मालूम होता है — ले बाबुल, अपना घर संभाल. तू जाने तेरा काम जाने. मैंने तो तेरे आँगन में जैसा जंचा, खेल लिया.
श्री महेन्द्र मोदी का यह लेखन बरबादियों का जश्न है. आप न भी चाहें तब भी यह पुस्तक आपको हाथ पकड़कर इस जश्न में शामिल होने के लिए खींच लायेगी.
जनवरी, 2021